चुम्बकत्व एवं विद्युत चुम्बकत्व (Magnetism and Electro Magnetism)
चुम्बकत्व एवं विद्युत चुम्बकत्व (Magnetism and Electro Magnetism)
प्राचीन काल में मैग्नेशिया के अन्दर एक पत्थर ऐसा पाया गया जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था. बाद में इस
U आकार अधिकतर मूविंग क्वाइल उपयन्त्रों में प्रयोग किए जाते हैं। रिंग आकार के चुम्बक स्पीकर में और कई सारे एक साथ ड्रम पर चिपका कर पत्थर पर और प्रयोग किये गए. देखा गया कि यह स्वतन्त्रता पूर्वक फाउण्ड्री इत्यादि में मिट्टी में से लोहे के कण अलग करने के लिए उपयोगटकाने पर उतर व दक्षिण दिशा में ही ठहरता है तथा ऊंचाई से गिराने इ गर्म करने से अपने चुम्बकीय गुण खो देता है। उस स्थान के नाम पर ही इसका नामकरण मैगनेट रखा गया।
चुम्बक का वर्गीकरण (Classification of Magnets)
चुम्बक को निम्नलिखित दो वर्गों में बाटा गया है -
(a) प्राकृतिक चुम्बक (Natural Magnet)
(b) कृत्रिम चुम्बक (Artificial Magnet)
(C) प्राकृतिक चुम्बक (Natural Magnet)
यह पत्थर के रूप में लोहे का ऑक्साइड (Feg,O) होता है। इसे लीडिंग स्टोन भी कहते हैं क्योंकि यदि इसे धागे से बांध कर लटकाया जाए तो यह उतर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जो सिरे अर्थात जिन पर अधिकतम चुम्बकीय शक्ति होती है वह सिरा चुम्बक का ध्रुव कहलाता है। जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है वह उत्तरी ध्रुव (North Pole) और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाला ध्रुव दक्षिण ध्रुव (South Pole) कहलाता है। चुम्बक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान बुद एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
कृत्रिम चुम्बक (Artificial Magnet)
चूंकि प्राकृतिक चुम्बक की शक्ति बहुत कम होती है इसलिए उपयोगी कार्यों में इसका उपयोग सीमित है। अतः कठोर स्टील द्वारा तैयारकिये गये चुम्बक जिनकी शक्ति प्राकृतिक चुम्बक की अपेक्षा अधिक होती का उपयोग अधिक किया जाता है। ये कृत्रिम चुम्बक कहलाते हैं।
कृत्रिम चुम्बक के प्रकारये दो प्रकार के होते हैं।
(i) स्थाई चुम्बक
(ii) अस्थाई चुम्बक
स्थाई चुम्बक (Permanent Magnets) :-
ये चुम्बक कठोर स्पात से बनाए जाते हैं जो लम्बे समय तकचुम्बकीय गुण ग्रहण किए रहते हैं। ये अधिकतर छड़ चुम्बक(BarMagnets), हार्सशू चुम्बक (Horse Shoe Magnets), यू आकार (UShaped), रिंग आकार (Ring Shaped) व बेलननुमा (Cylindrical Magnet) के आकारों में बनाए जाते हैं। इनमें प्रयुक्त पदार्थ अधिकतर कोबाल्ट, स्पातव टंगस्टन स्पात होता है।
उपयोग :-
स्थाई चुम्बकों में छड़ चुम्बक प्रयोगशालाओं में तथा हार्स-शू या बेलन आकार के स्थाई चुम्बक मूविंग कवाइल उपयन्त्रों में एल्यूमिनियम फर्म के अन्दर क्रोड के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं।
अस्थाई (Temporary Magnet) :-
ये चुम्बक एक नर्म लोह क्रोड को इन्सुलेटिड बना कर उस पर विधुत रोधी चालक तार लपेट कर बनाए जाते हैं। जब क्रोड पर लिपटी कुण्डली में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह नर्म लोह क्रोड चुम्बक बन जाती है, जो छड़ चुम्बक की तरह कार्य करती है। अतः सभी प्रकार के विद्युत चुम्बक अस्थाई चुम्बक कहलाते हैं क्योंकि जैसे ही इस कुण्डली में से धारा प्रवाह को रोक लेते हैं तो कुण्डली के अन्दर रखा नर्म लोहे का टुकड़ा अपना चुम्बकीय गुण खो देता है।
उपयोग :-
इलैक्ट्रोमैगनेट सभी विद्युत मशीनों मे, विद्युत घण्टी, पंखे, इत्यादि
में और भार उठाने में उपयोग
स्थाई चुम्बक बनाने की विधियां :-
निम्नलिखित तीन विधियां मूल विधियां हैं जिन से छड़ चुम्बक
बनाए जा सकते हैं।
(i) स्पर्श विधि
(ii) विद्युत धारा द्वारा
(iii) प्रेरण द्वारा
इसे फिर निम्न तीन विधियों में बांटा गया है।
(a) एकल स्पर्श विधि (Single Touch Method)
(b) दोहरी स्पर्श विधि (Double Touch Method)
(c) विभाजित स्पर्श विधि (Divided Touch Method)
(a) एकल स्पर्श विधि (Single Touch Method)
इस विधि में स्पात की छड़ को जिसे चुम्बक बनाना है, लकड़ी के गुटके के उपर रखें। अब एक स्थाई छड़ चुम्बक के उत्तरी सिरे को स्पात छड़ के एक सिरे से स्पर्श करते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएँ और दूसरे सिरे पर जाकर चुम्बक को ऊपर उठाएँ और पुनः पहले सिरे से दूसरे सिरे की ओर रगड़ते हुए ले जाएँ। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएँ जब तक स्पात छड़ चुम्बक न बन जाए।
(b) दोहरी स्पर्श विधि (Double Touch Method):-
इस विधि में स्पात की छड़ दो छड़ चुम्बक के सिरों पर रखी जाती हैं जिनके विपरित ध्रुव एक दूसरे के सामने हों। चित्र के अनुसार स्पात छड़ को रख कर स्पात छड़ के मध्य एक लकड़ी का गुटका रखा जाता है। फिर दो अन्य छड़ चुम्बक जिनके ध्रुव भिन्न भिन्न हों लकड़ी के टुकड़े से स्पर्श करते हुए स्पात छड़ के खाली सिरों की तरफ रगड़ते हुए
(c) विभाजित स्पर्श विधि (Divided Touch Method):- इस विधि में दो विपरीत ध्रुव सिरे वाले छड़ चुम्बक दोहरे स्पर्श विधि की तरह स्पात छड़ के मध्य में रखें, दोनों के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव स्पर्श करें, स्पात छड़ दो छड़ चुम्बकों के उपर रखी हो जिनके विपरित सिरे आमने सामने हों। स्पात छड़ के मध्य लकड़ी का गुटका नहीं हो और रगड़ने वाले चुम्बकों को स्पात छड़ के मध्य सिरे से अन्तिम सिरे तक ले जाएँ और अन्तिम सिरे से ऊपर उठाकर पुनः स्पात छड़ के मध्य सिरे को स्पर्श करें और फिर स्पात छड़ के अन्तिम सिरे तक ले जाएँ।
(ii) विद्युत धारा द्वारा (By Electric Current) :- इस विधि में स्पात की छड़ को विद्युत रोधी बनाकर उस पर इन्सुलेटिड इनेमल्ड तार की कुण्डली लपेट कर दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर स्पात की छड़ शक्तिशाली चुम्बक बन जाती है। यदि यह स्पात छड़ नर्म लोहे की है तो यह तब तक चुम्बकीय बनी रहती है जब तक कुण्डलीमें धारा प्रवाहित रहती है। यदि धारा प्रवाह रोक लिया जाए तो छड़ चुम्बकत्व समाप्त हो जाता है। यदि स्पात छड़ कठोर स्पात की होगी तो धारा प्रवाह हटाने पर भी छड़ में चुम्बकत्व रह जाता है। इस प्रकार चुम्बक का उपयोग काफी व्यापक है।
(iii) प्रेरण द्वारा (By Induction Method) :- इस विधि द्वारा चुम्बकों का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। इस विधि में पोल चार्जर का उपयोग किया जाता है। पोल चार्जर एक शक्तिशाली विद्युत चुम्बक होता है जो कि बहुत अधिक टन से कुण्डलित होता है। चार्जर की कुण्डली के मध्य एक लोह क्रोड होती है। जिस स्पात छड़ को चुम्बक बनाना होता है उसे चार्जर की उपरी सतह पर रखते हैं और चार्जर को दिष्ट धारा से पुश बटन की सहायता से थोड़े समय के लिए ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके मध्य रखी लोह की छड़ भी चुम्बक बन जाती है। यह चुम्बकीय प्रेरण द्वारा होता है। पोल चार्जर का स्विच ऑफ करने के पश्चात लोह छड़ हटा दी जाती है। इस विधि के निम्नलिखित लाभ हैं।
(a) इस विधि से स्टील के छोटे टुकड़े भी चुम्बक बनाये जासकते है
(b) इसमें समय बहुत कम लगता है।
(c) किसी भी आकार का स्पात का टुकड़ा चुम्बक बनाया जा सकता है।
इस विधि द्वारा स्पीकर, टेलीफोन, माइक्रोफोन, इयर फोन, विद्युत उपयन्त्रों और मैगनेटो इत्यादि के चुम्बक बनाए जाते हैं।
पोल चार्जर चुम्बकत्व का आणविक सिद्धान्त (Molecular Theory of Magnetism):-
सन् 1852 में श्रीमान् वेबर ने इस सिद्धान्त को आगे किया कि सभी चुम्बकीय पदार्थों के अणु पूर्ण चुम्बक होते हैं और प्रत्येक अणु में एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके बाद सन 1890 में ऐविंग (Ewing) ने इसे और आगे विकसित किया, इसलिए इसे वेबर और ऐविंग अणु थ्योरी भी कहते हैं।
चुम्बकीय पदार्थों में चुम्बकीय अणु यदृच्छ ढंग (Haphazard manner) में विभिन्न दिशा व ग्रुप में पड़े रहते हैं। जब तक ऐसे पदार्थों को चुम्बकीय क्षेत्र में न लाया जाए तो ये चित्र 11.7(a) की भांति विभिन्न दिशाओं व ग्रुप में पड़े रहते हैं और इनका परिणामी चुम्बकत्व शून्य होताहै ।
एक लोह पदार्थ में अणु चुम्बक का विन्यास
जब लोह छड़ को किसी शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है या लोह छड़ को एक स्थाई चुम्बक के उत्तरी ध्रुव से रगड़ा जाता है तो प्रत्येक अणु अपने पुराने ग्रुप को छोड़ कर स्थाई चुम्बक के उत्तरी ध् ध्रुव की तरफ आकर्षित होते हैं और प्रत्येक चुम्बकीय अणु अपना दक्षिणी ध् ध्रुव वाला सिरा स्थाई चुम्बक के उत्तरी ध्रुव की ओर करता है। परिणाम स्वरूप चित्र 11.7 b की भांति सभी चुम्बकीय अणु एक निश्चित दिशा में ग्रुप बनाते हुए व्यवस्थित हो जाते हैं और लोह छड़ का एक सिरा उत्तरी ध्रुव व दूसरा दक्षिण ध्रुव बन जाता है।
चुम्बकीय पदार्थ (Magnetic Materials) :-
पदार्थों की वह श्रेणी जो चुम्बक द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, उसे चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। इनको निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
(i) लोह-चुम्बकीय (Ferro-magnetic) :-
जिन पदार्थों में चुम्बकीय गुण बहुत अधिक होते हैं, वे लोह चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें सरलता से चुम्बक बनाया जा सकता है। इनकी चुम्बकशीलता बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्पात और इनसे बनी मिश्र धातुएँ इस श्रेणी में आती हैं।
(ii) समचुम्बकीय (Paramagnetic) :-
जिन पदार्थों में चुम्बकीय गुण कम होते हैं, वे समचुम्बकीय या अनुचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की चुम्बकशीलता इकाई से थोड़ी अधिक होती है। इन्हें बहुत मामूली रूप से चुम्बकित किया जा सकता है। इन पदार्थों में एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम, क्राउन ग्लास, मैग्नेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन आदि आते हैं।
(iii) विषम चुम्बकीय (Diamagnetic) :-
जो पदार्थ बिल्कुल भी चुम्बक नहीं बनाए जा सकते, प्रतिचुम्बकीय या विषम चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चुम्बकशीलता इकाई से कम होती है। ये पदार्थ चुम्बक से आकर्षित नहीं होते अपितु कुछ प्रतिकर्षित ही होते हैं।
विशेष नोट :-
(i) वे पदार्थ जिनकी चुम्बकशीलता उच्च और अवशिष्ट चुम्बकत्व कम होता है. कोमल चुम्बकीय कहलाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग पटलित क्रोड बनाने के लिया किया जाता है।
(ii) जिन पदार्थों की पलस्क डेनसिटी B उनके क्षेत्र सामर्थ्य से अधिक हो और प्रतियास उच्च हो, कठोर चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों से स्थाई चुम्बक बनाए जा सकते हैं। इनमें टंगस्टन, स्टील, एलनिको व कोबाल्ट स्टील प्रमुख हैं।
कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ :-
चुम्बकीय प्रेरण (Magnetic Induction) :-
यदि किसी चुम्बक के पास कोई चुम्बकीय पदार्थ रखा जाए तो चुम्बक के चुम्बकीय क्षेत्र में चुम्बकीय बल रेखाएँ इस चुम्बकीय पदार्थ को भी अपना माध्यम बना लेती हैं और यह भी चुम्बक बन जाता है। यह घटना चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। नीचे चित्र में इसे दिखाया गया है।
चुम्बकीय बल (Magnetic Force)
किसी चुम्बक को चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर चुम्बक द्वारा अनुभव किया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, चुम्बकीय बल कहलाता है।
चुम्बकीय बल के नियम
कूलम्ब के नियमानुसार
(1) दो बिन्दु ध्रुवों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल प्रत्येक ध्रुव की सामर्थ्य के समानुपाती होता है।
(2) दो बिन्दु ध्रुवों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है।
यह बल दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के साथ एक ओर से।
दूसरी ओर तक कार्य करता है।
प्रेरण द्वारा लोह छड़ का चुम्बक बनना चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic Field) :-
किसी चुम्बक के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक चुम्बकीय बल रेखाओं को अनुभव किया जा सके, उस चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। चित्र 11.9 में एक छड़ चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र दिखाया गया है।
चुम्बकीय बल रेखाऐं
चुम्बकीय क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :-
(i) किसी नर्म लोहे के टुकड़े को इस चुम्बकीय क्षेत्र में रखने से वह प्रेरण द्वारा चुम्बक बन जाता है।
(ii) किसी अन्य चुम्बक को इस क्षेत्र में रखने से वह बल का
अनुभव करता है।
(iii) यदि किसी चालक द्वारा बनी बन्द कुण्डली इस क्षेत्र में रख कर घुमाई जाए तो इसके द्वारा बल रेखाओं के कटने से कुण्डली में वि
वा. बल उत्पन्न हो जाता है।
(iv) यदि इस क्षेत्र में कोई धारा वहन करता हुआ चालक रखा जाए तो वह बल का अनुभव करता है।
चुम्बकीय फ्लक्स (Magnetic Flux) :-
किसी चुम्बकीय क्षेत्र की कुल चुम्बकीय बल रेखायें उस क्षेत्र का
बकीय फ्लक्स कहलाती है। इसकी इकाई वेबर है और इसे ग्रीक अक्षर (Ph) से दर्शाया जाता है।
मैक्सवेल (Maxwell) :-
एक मैक्सवेल इकाई एक चुम्बकीय रेखा होती है। चित्र 11.11 से दिखाया गया है कि छ चुम्बकीय बल रेखाऐं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव ओर जा रही हैं तो हम कह सकते हैं कि इस चुम्बक के क्षेत्र में 6 बेकसवेल फ्लक्स है। यह इकाई जेम्स क्लार्क मैकसवेल के नाम पर रखी गयी है जो (1831-1879) के बीच प्रसिद्ध स्कोटीस भौतिक गणितज्ञ हुए
यह चुम्बकीय फ्लक्स की बड़ी इकाई है। एक वेबर 1x10# मेक्सवेल या चुम्बकीय बल रेखाओं के बराबर होता है। यह इकाई विलहेम वेबर के नाम पर रखी गई है, जो कि (1804-1890) में महान जर्मन
वैज्ञानिक हुए हैं।
गास (The Gauss) :-
यह COS प्रणाली में फ्लक्स घनत्व की इकाई है जो एक चुम्बकीय बल रेखा प्रति वर्ग रोगी होती है। Mx/cm/'/ उदाहरण के लिए ऊपर चित्र 11.11 में कुल पलक्स 6 लाईनों का है या इसे 6Mx कह सकते है। P बिन्दु पर यह पलक्स घनत्व 20 है क्योंकि यहां प्रति वर्ग सेन्टी मीटर में केवल 2 लाइनें हैं। चुम्बकीय पोल के पास फ्लक्स घनत्व अधिक होता जहां पर बल रेखाएँअधिक सघन होती है। यह इकाई प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ कार्ल एफ गास Karl F. Gauss के नाम पर रखी गई हैं जो 1777 से 1855 के बीच हुए हैं।
निरपेक्ष चुम्बकशीलता (Absolute Permeability) :-
किसी चुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय बल रेखाओं की अपने अन्दर संचालन क्षमता को उस पदार्थ की निरपेक्ष चुम्बकशीलता कहते हैं अथवा फ्लक्स घनत्व B और क्षेत्र तीव्रता H में अनुपात को भी निरपेक्ष चुम्बकशीलता कहते हैं। इसे प्र. से दर्शाते हैं।
अतः निरपेक्ष चुम्बकशीलता H. -पेक्ष चुम्बकशीलता मुक्त अन्तराल की चुम्बकशीलता व माध्यम की चुम्बकशीलता के गुणनफल के बराबर होती है।
अर्थात = Ho, हेनरी प्रति मीटर। Ha
सापेक्ष चुम्बकशीलता (Relative Permeability) :-
किसी माध्यम की चुम्बकशीलता उस माध्यम की वायु की अपेक्षा बल रेखाओं की संचालन क्षमता होती है। इसे , से दर्शाते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती।
क्षेत्र सामर्थ्य (Field Strength) :-
किसी चुम्बकीय क्षेत्र में एक इकाई उत्तरी ध्रुव रखने पर ध्रुव पर कार्य करने वाले बल को उस क्षेत्र की क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। इसे क्षेत्र तीव्रता भी कहते हैं। इसे H से दर्शाया जाता है और इसकी इकाई न्यूटन प्रति वेबर या एम्पियर टर्न प्रति मीटर होती है।
चुम्बकीय बल रेखाएं (Magnetic Lines of Force) :-
ये वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जो चुम्बक के अन्दर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव व बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हुई मानी गई हैं। ये वक्र रेखाऐं ही चुम्बकीय बल रेखाएँ कहलाती हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं :-
(i) प्रत्येक चुम्बकीय बल रेखा एक बन्द परिपथ बनाती है। (ii) यह कभी भी परस्पर नहीं कटती।
(iii) ये तनी हुई लचीली डोरियों की तरह होती हैं जो कि स्वयं
= 100 लाइन या Mx के बराबर होता है। में सुकड़ने का प्रयत्न करती हैं।
फ्लक्स घनत्व (Flux Density)
किसी चुम्बकीय क्षेत्र के इकाई लम्बवत क्षेत्र में से गुजरने वाले
फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व कहते हैं ।
यदि किसी चुम्बकीय क्षेत्र जैसा कि चित्र 11.11 में दिखाया गया
है वेबर सम्पूर्ण फ्लक्स A वर्ग मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्र में से गुजरता है तो
फ्लक्स घनत्व B =वेबर प्रति वर्गमीटर होगा इसे B से दर्शाया जाता है
चुम्बकीय घूर्ण (Magnetic Moment) :-
चुम्बक की लम्बाई और पोल की सामर्थ्य के गुणनफल को उस चुम्बक का चुम्बकीय घूर्ण कहते हैं। इसे M से दर्शाते हैं और इसकी इकाई वेबर मीटर होती है।
धारणशीलता (Retentivity) :-
किसी चुम्बकीय पदार्थ को चुम्बकीय क्षेत्र के बल से दूर हटा लेने के बाद भी चुम्बकत्व धारण रखने की प्रवृत्ति उस पदार्थ की रिटेनटीविटी या धारणशीलता कहलाती है।
चुम्बकीय ग्रहणशीलता (Magnetic Susceptibility) :- चुम्बकीय पदार्थों को चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर प्रेरण द्वारा चुम्बकत्व बनने की प्रवृत्ति उस पदार्थ की ग्रहणशीलता कहलाती है. यह क्षेत्र की तीव्रता | और क्षेत्र सामर्थ्य H का अनुपात होती है। इसे K से दर्शाया जाता है और इसकी इकाई हेनरी प्रति मीटर होती है।
अतः: K = हेनरी प्रति मीटर
विद्युत चुम्बकत्व (Electro Magnetism) :-
विद्युत व चुम्बकत्व के बीच सम्बंध सर्वप्रथम ओरस्टड ने सन 1824 में खोजा। उसने पाया कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है और उसके पास चुम्बकीय सुई लाते हैं तो वह विक्षेप करती है। इसके कुछ वर्षों बाद इसके विपरीत प्रभाव का पता लगा कि यदि किसी चालक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र घुमाया जाये तो चालक में विवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रभाव अंग्रेज भौतिक विज्ञानी और इलैक्टोमैगनेटिजम के अन्वेषक माइकल फैराडे (1791-1867) ने खोजा। इसके अतिरिक्त अमेरिकन भौतिक विज्ञानी जोसेफ हेनरी (1797-1878) तथा रूसी भौतिक विज्ञानी एच.एफ.ई.लैन्ज (1804-1865) ने भी महत्वपूर्ण खोज की।
एक सीधे चालक में धारा प्रवाह के कारण चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic Field Due to Straight Current Carrying Conduc- tor) :-
यदि किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाह करके उसके पास चुम्बकीय सुई लाएँ तो यह विक्षेप दर्शाती है जिससे मालूम पड़ता है कि विद्युत धारा के कारण चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चित्र 11.12 (a) व चित्र 11.12 (b) में चालक में विद्युत धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र दिखाया गया है जिसके अन्य प्रभाव निम्नलिखित होते हैं:-
सुई एक विशेष दिशा में तथा चालक के दूसरी तरफ रखने पर सुई पहले की विपरीत दिशा में संकेत करती है।
(iii) चुम्बकीय बल रेखाएँ हमेशा चालक के चारों ओर वृताकार रूप में विद्यमान रहती हैं और इन वृतों का केन्द्र चालक के केन्द्र पर होता है। (iv) चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर चुम्बकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है जिससे सिद्ध होता है कि चालक में धारा की दिशा बदलने से चुम्बकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी बदलती है। (v) चालक में धारा का मान बढ़ाने से चुम्बकीय सुई का विशेष भी तेजी से होता है।
(vi) चालक के पास सुई का विक्षेप अधिक तेजी से तथा चालक से सुई दूर ले जाने पर सुई का विक्षेप कम होता जाता है।
विद्युत धारा द्वारा बने चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा (Mag-netic Field Due to Electric Current) :-
इस सम्बन्ध को निम्नलिखित नियमों से ज्ञात कर सकते हैं-
(i) दाहिने हाथ का नियम (Right Hand Rule) :-
यदि एक सीधे चालक को दाहिने हाथमें इस प्रकार पकड़ा जाए कि अगूंठा धारा की दिशा में हो तो अगुलियों की लपेट की दिशा चुम्बकीय बल रेखाओं को दर्शाएगी।
(ii) मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम (Maxwell's Cork Screw Rule)
(i) चुम्बकीय सुई की सुई हमेशा धारा की दिशा से लम्बवत होती है। (ii) चुम्बकीय सुई को चालक के एक तरफ रखने पर उसकी
चित्र -11.14
पेच को लकड़ी के ब्लाक में कसा जाये तो कसते समय पेच की दिशा यदि यदि दाहिने हाथ में पेचकस को पकड़ कर लकड़ी में कसने वाले धारा की दिशा बताये तो पेच के घूमने की दिशा चुम्बकीय बल रेखाओं कोbदर्शाएगी।
विशेष :-
पेच को पेच हैड की तरफ से देखने पर धारा की दिशा को तथा पेच को नोक की ओर देखते हैं अर्थात कल्पना करते हैं कि धारा आपकी ।तरफ आ रही है तो उसका चिन्ह डाट से दर्शाया जाता है।
दो समानान्तर धारा वाही चालकों के कारण चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic Field Due to Two Parallel Current Carrying
यह एक खोखली इन्सुलेटिड बेलनाकार बोबिन पर इन्सुलेटिड ताम्र तारों से लिपटी एक कुण्डली होती है। इसमें तारों की एक तह या अधिक भी हो सकती है। इस कुण्डली में दिष्ट धारा गुजारने से यह छड़ चुम्बक जैसा व्यवहार करती है।
परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हाथ के नियम या कॉर्क स्क्रू नियम से ज्ञात कर सकते हैं।
(i) दक्षिण हस्त नियम से
यदि सोलेनॉइड को दांये हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियों की लपेट धारा की दिशा में हो तो अगुंठा परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और यह उत्तरी ध्रुव की तरफ संकेत होगा । (ii) कॉर्क स्क्रू नियम सेत्र
यदि कॉर्क स्क्रू को दांये हाथ से कसते समय यह कल्पना करें कि यदि धारा की दिशा स्क्रू के कसने की दिशा में है तो स्क्रू की आगे बढ़ने की दिशा चुम्बकीय बल रेखाओं की होगी अर्थात् परिनालिका के जिस सिरे से चुबल रेखाएं निकलेंगी वह सिरा उत्तरी ध्रुव होगा।
परिनालिका के अन्दर बल रेखाएं परिनालिका के अक्ष के समानान्तर चलती हैं परन्तु परिनालिका के बाहर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं।
चुम्बकत्व वाहक बल (Magneto Motive Force)
विद्युत परिपथ की भांति चुम्बकीय परिपथ में यह वह बल होता है जो चुम्बकीय फ्लक्स को स्थापित करवाता है। यह कुण्डली में लिपटी टनों और प्रवाहित धारा के गुणनफल के तुल्यहोता है। इसे प्राय: Ni से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई एम्पीयर टर्न होती है।
प्रतिष्टम्भ (Reluctance)
चुम्बकीय पदार्थों में यह पदार्थों का वह गुण है जो फ्लक्स प्रवाह का विरोध करता है। यदि किसी चुम्बकीय परिपथ की लम्बाई (मीटर और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A = वर्ग मीटर में, ॥ = मुक्त अन्तराल की चुम्बकशीलता हेनरी प्रतिमीटर में और 1, = सापेक्ष चुम्बकशीलता हो तो प्रतिष्टम्भ
परमीन्स (Permeance) :-
प्रतिष्टम्भ के विलोम को परमीन्स कहते हैं। यह चुम्बकीय पदार्थ
का वह गुण है जो चुम्बकीय परिपथ में फ्लक्स को प्रवाहित करने के लिए सहयोग करता है। यह विद्युत परिपथ में चालकता के अनुरूप है। इसकी इकाई वेबर प्रति एम्पीयर टर्न या हेनरी है।
लीकेज फ्लक्स (Leakage Flux) :-
प्रायोगिक रूप में जनित्र या मोटर में स्टेटर व रोटर के मध्य वायु अन्तराल रखा जाता है। स्टेटर फ्लक्स का अधिकांश भाग वायु अन्तराल को पार करके रोटर में पहुंचता है परन्तु वायु का प्रतिष्टम्भ अधिक होने के कारण फ्लक्स का कुछ भाग वायु अन्तराल को पार करके रोटर में नहीं पहुंचता। इस फ्लक्स को लीकेज या क्षरण फ्लक्स कहते हैं। नीचे 11. 23 चित्र में एक रिंग में प्रवाहित फ्लक्स व क्षरण फ्लक्स दिखाया गया है। वायु अन्तराल के पास फैला हुआ फ्लक्स जो वायु अन्तराल में से प्रवाहित नहीं होता फ्रिन्ज फ्लक्स कहलाता है। इसके कारण वायु अन्तराल का प्रभाविक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ जाता है।
वह फ्लक्स जो वायु अन्तराल को पार करके अपना परिपथ पूरा कर लेता है, उपयोगी फ्लक्स कहलाता है।
विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुम्बकीय फ्लक्स को सम्पूर्ण फ्लक्स कहते हैं।
निम्नलिखित विधियों से क्षरण फ्लक्स कम किया जा सकता
(i) वायु अन्तराल घटा कर
(ii) वायु अन्तराल के पास तांबे की एक्साइटेशन कुण्डली लपेट कर ।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction) :-
माइकल फैराडे (1791-1867) ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कुछ नियम स्थापित किए, जिन पर लगभग सभी विद्युत मशीने जैसे मोटर, जनित्र या ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं। फैराडे ने निम्नलिखित दो विद्युत
चुम्बकीय प्रेरण के नियम निर्धारित किए:-
प्रथम नियम :-
जब कोई चालक चुम्बकीय बल रेखाओं को काटता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है।
दूसरा नियम :-
चालक द्वारा चुम्बकीय बल रेखाओं के कटने से उत्पन्न वि.वा. बल का परिमाण फ्लक्स गंथन में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। i, मान लो कि किसी कुण्डली में N टर्न हैं और इसमें एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर , फ्लक्स उत्पन्न होकर गुथित होता है यदि कुछ समय । सैकिण्ड के बाद कुण्डली में धारा 12 प्रवाहित की जाए तो फ्लक्स गंथन 42 होगा। इस प्रकार फ्लक्स गुंथन के परिवर्तन की दर NQ2 –
लेंज का नियम (Lanz's Law) :-
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में किसी कुण्डली या चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है, जिसके कारण यह उत्पन्न होता है चाहे वह गति हो या किसी अन्य तरह का परिवर्तन हो।
फ्लेमिंग का दांये हाथ का नियम (Fleming's Right Hand Rule)
यह नियम चुम्बकीय फ्लक्स और चालक के सापेक्ष वेग के कारण उत्पन्न वि.वा.बल के सम्बन्ध को दर्शाता है। इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ को इस प्रकार पकड़ा जाए कि पहली अंगुली, मध्य अंगुली एवं अंगूठा परस्पर 90° पर हो तो, पहली अंगुली बल रेखाओं मध्य अंगुली धारा और अंगूठा गति की दिशा दर्शाता है।
गेल्वेनोमापी
चित्र 11.24 में दिखाया गया है कि स्थाई छड़ चुम्बक को जब कुण्डली की ओर लाया जाता है तो स्थाई चुम्बक द्वारा दिये गए फ्लक्स में जो कुण्डली से गुथित हो रहा था चुम्बक के आगे बढ़ने से परिवर्तन होता है और कुण्डली में वि.वा.बल उत्पन्न होता है जिसका प्रदर्शन गेलवेनोमापी ओर संकेत करके दिखाता है और कुण्डली में वही ध्रुव बनता है जो उसके सामने स्थाई चुम्बक का है और समान चुम्बक एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इसलिए स्थाई चुम्बक को कुण्डली की ओर आने में विपरित बल का सामना करना पड़ता है।
इस चित्र 11.25 में दिखाया गया है कि छड़ चुम्बक को कुण्डली से दूर ले जाया जा रहा है। इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और कुण्डली में भी वि.वा.बल उत्पन्न हुआ परन्तु गेल्वेनोमापी में संकेत पहले की अपेक्षा विपरीत है और धारा भी विपरीत प्रवाहित होने से अब कुण्डली की क्रोड की पहले वाली फलक दक्षिण ध्रुव बन जाएगी और चुम्बक को दूर ले जाने का विरोध होगा। इन बातों से सिद्ध होता है कि किसी कुण्डली या चालक में प्रेरित वि.वा.बल उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह पैदा होता है।
स्थैतिकतया उत्पन्न वि.वा.बल (Statically Induced
यदि किसी कुण्डली या परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चालकों के चारों ओर फ्लक्स स्थापित होकर उससे गुथित होता है और अब यदि प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाए तो गुथित फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है और कुण्डली में वि.वा.बल उत्पन्न हो जाता है। यह वि.वा.बल स्थैतिकतया उत्पन्न वि.वा.बल कहलाता है। यह दो प्रकार से हो सकता है :-
(i) परस्पर प्रेरित वि.वा.बल (Mutually Induced E.M.F.) (ii) स्वप्रेरित वि.वा.बल (Self Induced E.M.F.)








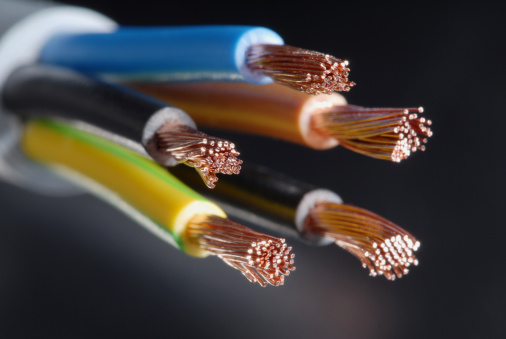
Comments
Post a Comment