विद्युत शक्ति का संचारण
विद्युत शक्ति का संचारण (Transmission of Electrical Power)
विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये अर्थात् संचारण और वितरण की मूलतः दो विधियाँ हैं-
(1) प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली (AC system)
(2) दिष्ट धारा प्रणाली (DC system)
(1) प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली की विशेषतायें- विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग AC में ही संचारण व वितरण किया जाता है। AC प्रणाली की निम्नलिखित विशेषतायें हैं-
(i) प्रत्यावर्ती धारा प्रदाय को 33 kv तक की उच्च वोल्टता में पैदा किया जा सकता है जबकि DC प्रदाय को उच्च वोल्टता में जनेरेट करना सरल नहीं है।
(ii) AC मशीनें DC मशीनों की अपेक्षा बनावट में सरल, सस्ती व टिकाऊ होती है।
(iii) AC में वोल्टता को ट्रांसफॉर्मर द्वारा सरलता से उच्च व निम्न कर सकते हैं जबकि DC में ऐसा सम्भव नहीं है।
प्रत्यावर्ती धारा के दोष-
। अतः इस प्रणाली में ताँबा या एल्यूमीनियम की बचत हो सकती है।
3. डी.सी. में त्वाचिक प्रभाव (skin effect) नहीं होता अत: चालक का सम्पूर्ण अनुप्रस्थ क्षेत्र उपयोग होता है।
4. डी.सी. प्रणाली में प्रेरकत्व धारित्र व कला विस्थापन समस्यानहीं होती
5. डी.सी. में इन्सुलेशन पर विभव प्रतिबल (Potential stress) AC की अपेक्षा 0.707 होता है। इस कारण समान वोल्टता के लिये DC में कम इन्सुलेशन की आवश्यकता होती है।
6. DC में उच्च वोल्टता लाइनें आवेशित नहीं होती।
7. DC में प्रेरणिक और धारित्र प्रभाव न होने के कारण लाइनवोल्टेज रेगूलेशन कम होता है।
8.भूमिगत केबलों में DC सप्लाई पर शीथ हानियाँ नहीं होती है।
(2) दिष्ट धारा प्रणाली की विशेषतायें-
1. डी.सी. संचारण में केवल दो चालकों की ही आवश्यकता
2. डी.सी. प्रणाली में भूमि (Earth) को वापसी (Returns) चालक के रूप में प्रयोग करके केवल एक चालक से भी ट्रांसमीशन
1. उच्च वोल्टता के कारण करंट कम हो जाता है और लाइन हानियां करंट पर निर्भर करती हैं। अत: उच्च वोल्टता ट्रांसमीशन में लाइन हानियां कम होती हैं।
2. लाइन वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाते हैं।
3. धारा कम होने से चालकों का व्यास कम हो जाता है जिससे
चालक पर व्यय कम हो जाता है।
4. संचारण दक्षता बढ़ जाती है।
दोष-
(i) उच्च वोल्टता पर डी सी पद्धति में जनरेशन करने पर
(i) प्रत्यावर्ती धारा प्रदाय पद्धति में प्रेरकत्व, धारित्र व फेज दिक्परिवर्तन (Commutation) की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विस्थापन और सर्ज वोल्टताओं आदि की समस्या रहती है।
(ii) AC में DC पद्धति की तुलना में संचारण व वितरण में चालकों का साइज अधिक लेना पड़ता है क्योंकि AC में त्वाचिक प्रभाव (Skin Effect) होता है।
(iii) प्रत्यावर्ती धारा प्रदाय में इन्सुलेशन अधिक रखना पड़ता है। (iv) AC में DC की तुलना में करोना प्रभाव अधिक होता है। (v) भूमिगत केबलों में AC के कारण सीथ हानियाँ अधिक
(ii) डी सी को उच्च व निम्न नहीं किया जा सकता।
नोट- उपरोक्त बिन्दुओं पर गौर करने पर पाया जाता है कि डी सी ट्रांसमीशन के लाभ अधिक हैं और यह लम्बी दूरी की संचारण लाइनों में किफायती भी है। इसलिये हमारे देश का अग्रणी संस्थान पावर ग्रिड कारपोरेशन लम्बी दूरी की उच्च वोल्टता की संचारण लाइनें डी सी प्रदाय के लिये उपयोग कर रहा है।
उच्च वोल्टता संचारण लाइनों के लाभ (Advantage of high voltage Trasmission line) :- अधिकतर जनन केन्द्र भार (vi)AC में प्रेरकत्व व धारित्र प्रभाव के कारण वोल्टेज रेगूलेशन केन्द्रों से बहुत दूर होते हैं और अधिक दूरी पर निम्न वोल्टेज पर विद्युत शक्ति का संचारण लाभदायक नहीं है
विद्युत शक्ति ट्रांसमीशन की विभिन्न पद्धतियाँ :
चूँकि अधिकतर AC शक्ति का संचारण तीन फेज तीन तार या तीन फेज चार तार प्रणाली में किया जाता है क्योंकि तीन फेज में एक फेज प्रणाली की अपेक्षा चालक व्यय कम होता है परन्तु विशेष परिस्थितियों में अन्य विधियों का भी उपयोग किया जाता हैँ ये विधियाँ निम्नलिखित प्रकार की हैं-
1. तीन फेज AC प्रणाली-
(a) तीन फेज तीन तार प्रणाली
(b) तीन फेज चार तार प्रणाली
2. दो फेज AC प्रणाली-
(a) दो फेज चार तार प्रणाली
(b) दो फेज तीन तार प्रणाली
3. एक फेज AC प्रणाली-
(a) एक फेज दो तार प्रणाली
(b) मध्य बिन्दु भू-सम्पर्कित एक फेज दो तार प्रणाली
4. दिष्ट धारा पद्धति-
(a) दिष्ट धारा दो तार प्रणाली
(b) मध्य बिन्दु भू-सम्पर्कित (Center Earthedpoint) डी.सी. दो तार प्रणाली
(c) दिष्ट धारा तीन तार प्रणाली।
शिरोपरी लाइनें (Over Head Lines ) :- शिरोपरी लाइनों में शक्ति का संचारण ACSR के नंगे चालकों द्वारा होता है। ये चालक लकड़ी, स्पात, RCC के खम्भे या जालदार स्पात के बुर्जों पर क्रास आर्म लगाकर, आर्म पर इन्सुलेटर लगाकर बंधे होते हैं। शिरोपरी लाइनों में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी - 4th सेमेस्टर R.P.
निम्नलिखित सामग्री प्रयोग की जाती है-
1. चालक (Conductor)
2. आधार (Support)
3. इन्सुलेटर (Insulator)
4. क्रास आर्म व क्लैम्प (Cross Arm and Clamp)
5. स्टे व स्टॉर्ट
6. गार्ड तार (Guard Wires)
1. चालक (Conductor) : सामान्यतया शिरोपरी लाइनों में
निम्नलिखित प्रकार के चालक प्रयोग किये जाते हैं- (a) ताँबा चालक
(b) एल्यूमीनियम चालक
(c) गेलवेनाइज्ड स्पात और लौह चालक
(d) एल्यूमीनियम कन्डक्टर स्टील रेनफोर्ड
(a) ताँबा चालक (Copper Conductor) :- विद्युत शक्ति संचारण व वितरण में सामान्यतया कर्षित कठोर (Hard drawn) ताँबा प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अम्लीकृत (Annealed) ताँबे से अधिक होती है। निम्नलिखित गुणों के कारण ताँबे के चालक प्रयोग किये जाते हैं-
(i) इनकी चालकता उच्च होती है।
(ii) ये चालक समरूप (Homogeneous) होते हैं। (iii) इनका धारा घनत्व उच्च होता है। (iv) इनकी तनन सामर्थ्य उच्च होती है।
(v) इनमें संक्षारण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है।
(vi) विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है





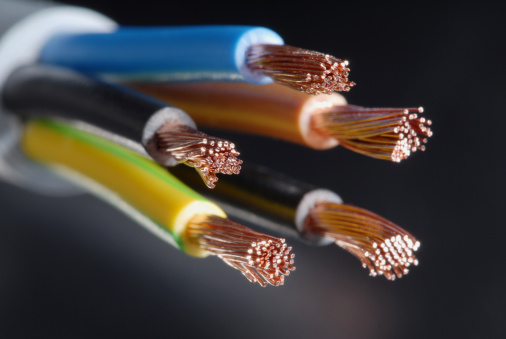
Comments
Post a Comment